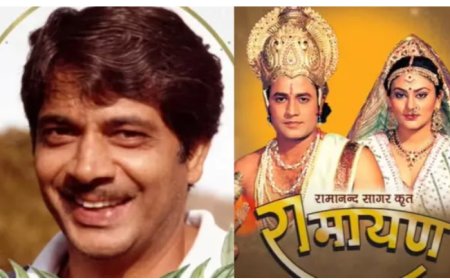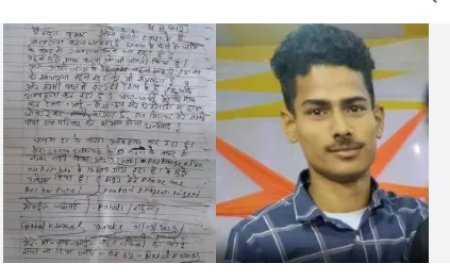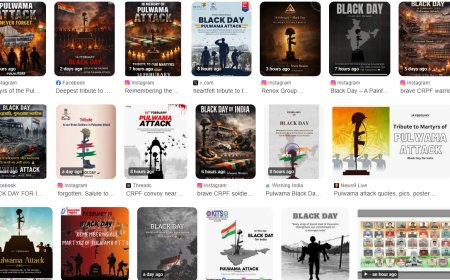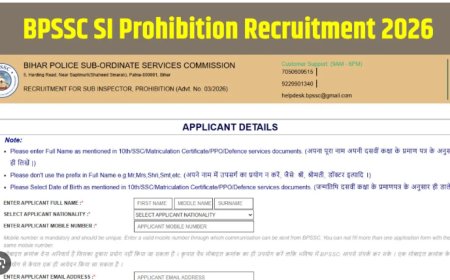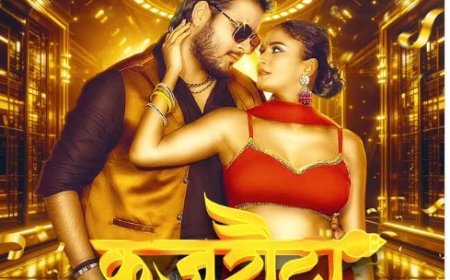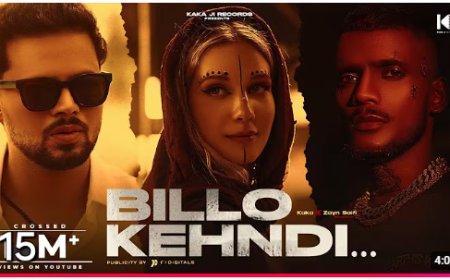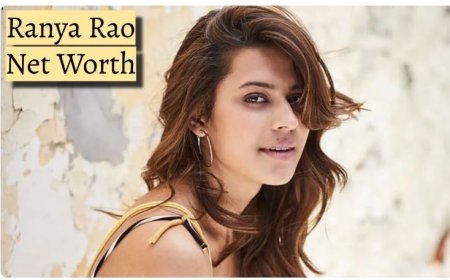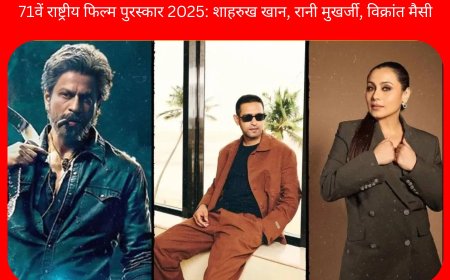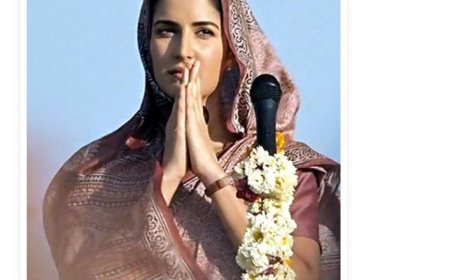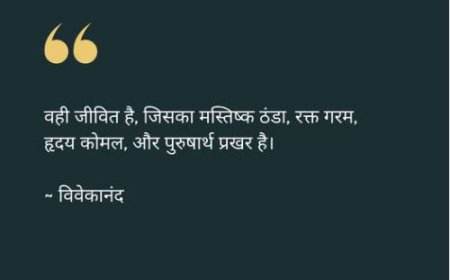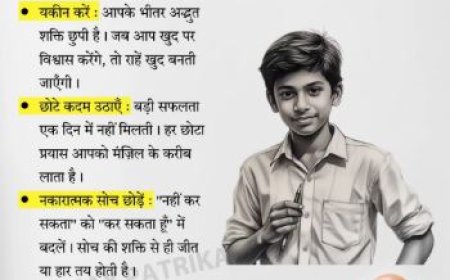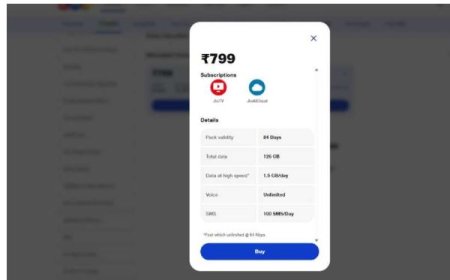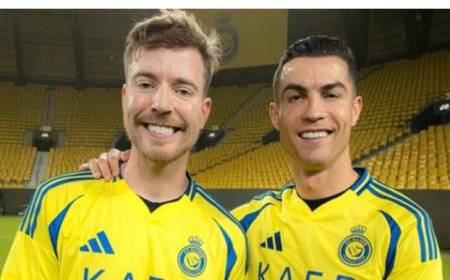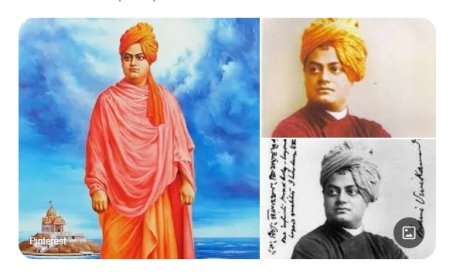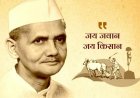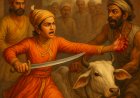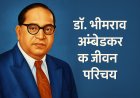भारत की पहचान - गिरीश्वर मिश्र book
Identity of India Girishwar Mishra book
भारत की पहचान
"भारतवर्ष' नाम से प्रसिद्ध हमारा देश आज एक लोकतंत्र के रूप में स्थापित है और संविधान के अनुसार यहाँ का शासन-तंत्र जन-कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अंग्रेजों के औपनिवेशिक राज से राजनैतिक मुक्ति पाने के बाद पिछले सात दशकों में देश ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति दर्ज की है। पर भारत देश सहस्रों वर्ष पुराना है और उसके अस्तित्व को पूरी परंपरा में देखे बिना समझना न संभव है और न समीचीन। "भारत राष्ट्र' और 'भारतीयता' को केवल वर्तानवी शासन और अंग्रेजी शिक्षा की देन मान बैठना किसी भी तरह ग्राह्य नहीं है तथापि इन्हें लेकर समकालीन चिंतन में अनेक प्रकार से विचार किया जा रहा है। भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से किए जा रहे देश-चिंतन में पर्याप्त विविधता दिखती है जो 'भारत' और उससे जुड़े देश-काल का विविधवर्णी चित्र उपस्थित करती है जिसमें शंका और संदेह के भाव भी दिखते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में भारत को भारत की दृष्टि से देखना और समझना हमारे सम्मुख एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया है। पंडित विद्या निवास मिश्र भारतीय चिंतन परंपरा के निष्णात विद्वान थे और उन्होंने उसके विविध पक्षों का प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत किया है। विशेष रूप से उन्होंने अपने निबंधों में सामान्य पाठकों के लिए अनेक प्रश्नों पर सरल और प्रवाहपूर्ण ढंग से प्रकाश डाला है। इस दृष्टि से उनके निबंधों का यह संकलन तैयार किया गया है। यहाँ पर इस प्रकार के प्रकाशन के प्रयोजन पर कुछ विस्तार में विचार करना उचित जान पड़ता है।
उल्लेखनीय है कि इन दिनों भारत की अस्मिता और चेतना को लेकर एक सजगता दिख रही है। मद्रास को 'चेन्नई', पांडिचेरी को 'पुदुच्चेरी', कलकत्ता को 'कोलकाता', उड़ीसा को 'ओडिशा' और बैंगलोर को 'बेंगलुरु' का नामकरण सांस्कृतिक चेतना की वापसी का परिचय दे चुके हैं। किसी भी देश की अस्मिता के लिए इस प्रकार के बदलाव प्रतीकात्मक होते हुए भी स्वतंत्रता और स्वायत्तता का बोध कराते हैं और उसके प्रति संवेदनशीलता को चिह्नित करते हैं। अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन में पराभव के फलस्वरूप विजयी और विजित के बीच शोषक भूमिका में आकर विजित समुदाय का उपयोग अपने हितों को साधने में करते हैं। वे आर्थिक दोहन करते हैं और विजित देश की जनता को भौतिक तथा मानसिक यातना और अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे विजित समुदाय के मानसिक धरातल पर भी आक्रमण करते हैं। अंततः वे विजित समाज के दृष्टिकोण और जीवन-शैली को बदलते हैं। विजयी देश ऐसी स्थिति में होता है कि उसकी प्रतिष्ठा विजित समुदाय के न केवल खान-पान व पहनावा जैसे जीवन के बाह्य पक्षों को ही प्रभावित करे बल्कि भाषा, साहित्य, सोचने का तरीका आदि सब कुछ उसके प्रभाव में आ जाते हैं। ज्यों-ज्यों समय बीतता है विजित समुदाय का विजयी के साथ संपर्क बढ़ता है और क्रमशः दोनों के बीच पहले अनुभव की जाने वाली भिन्नता और भौतिक-सांस्कृतिक दूरी घटने लगती है। भारत में अंग्रेजी राज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। अपने औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों ने न केवल भारत की अर्थ-संपदा का दोहन किया चल्कि आधुनिक भारतीय मानस को भारतीय ज्ञान-संपदा से विरक्त-सा बना दिया।
बदलती परिस्थितियों में विजित समुदाय के मन में अपनी सुरक्षा और विकास की चिंता एक महत्वपूर्ण सरोकार बन जाती है। ऐसे कमजोर क्षण में विजयी की ही तरह दिखने और जीने की लालसा प्रबल होने लगती है। ऐसे में लोग पराए को अपनाने और अपने को पराया वनाना शुरू कर देते हैं। वस्तुतः विजित समुदाय के लोग विजयी वर्ग के साथ अपनी समानता की तलाश शुरू करते हैं। अंततोगत्वा विजयी की ही तरह हो जाने की इच्छा तीव्र हो जाती है। इस क्रम में विजित समुदाय पुरानी कड़वी यादों को भुलाकर विजयी का अनुकरण करने लगता है। ऐसा करते-करते उसके मन में उन्हीं जैसा हो जाने की भावना उठने लगती है। इस तरह का मानसिक रूपांतरण करने के कई तात्कालिक लाभ भी दिखते हैं। पद, सम्मान, सुविधा और प्रतिष्ठा मिलने की संभावना दिखने लगती है। यह सब करते हुए सांस्कृतिक विस्मरण और अपनी पहचान को उधार की पहचान द्वारा पुनः परिभाषित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमें यह आभास ही नहीं होता कि कब क्या हो रहा है। यह बदलाव बड़ा व्यापक होता है। हम विजयी की वस्तुओं, विचारों, आचरण और व्यवहार आदि को देखकर विजयी जैसा होने की चेष्टा करने लगते हैं। समय बीतने के साथ पराभव की पीड़ा के साक्षी लोगों की संख्या भी घटने लगती है। चूंकि स्मति स्वभाव से रचनात्मक होती है नई पीढी के पास पीडा के दंश की
भूमिका
वह विजित समुदाय के भविष्य का रास्ता भी तय करने लगता है। रास्ता तय करने के उसके अपने उद्देश्य होते हैं और वे अपना आर्थिक-राजनैतिक हित साधने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। वे इसके लिए अवसर पैदा करते हैं। उनके द्वारा मानसिक उपनिवेश में जिस तरह के विवारों की खेती होती है, जो पौधे वा वृक्ष पनपते और बढ़ते हैं, जो फूल आते हैं उनका प्रकट संदर्भ विदेशी होता है। संस्कृतियों का सहज पारस्परिक संपर्क होने पर वेशभूषा, खानपान, रहन-सहन, सोच-विचार सभी में बदलाव आता है। पर जब वह किसी विजेता द्वारा आयातित और घोपा हुआ होता है तो वह सहज नहीं रह जाता। आरोपित संस्कृति के वर्चस्व से मूल संस्कृति के लोगों के सोचने का खाका, शब्द तथा वस्तुएँ सभी कुछ गिरवी रख जाते हैं। उन पर पटाक्षेप हो जाता है, वे इतिहास हो जाते हैं या उन्हें मिथक कहकर भ्रम की श्रेणी में रख दिया जाता है। उनकी अपनी देशज व्याख्या शंका के दायरे में खड़ी कर दी जाती है। विजेता श्रेष्ठता का प्रतीक बन जाता है और जो कुछ उसका अपना है यह उसे उचित ठहराते हुए विजित पर निर्भय भाव से आरोपित करने लगता है।
स्मरणीय है कि राजनैतिक और आर्थिक सत्ता के प्रभाव थोड़े दिनों तक ही रहते हैं, पर मानसिक रूप से जो हस्तक्षेप होते हैं वे बड़े प्रचल और दूरगामी प्रभाव बाले होते हैं। भारत में अंग्रेजी शासन और उनकी शिक्षा नीति ने यही किया। अंग्रेजी शिक्षा के सूत्रपात के साथ विषय वस्तु का जो विस्तार हुजा, सिद्धांतों और विधियों का प्रसार हुआ वह स्वदेशी विचारों, सिद्धांतों और विधियों के अस्वीकार और नकार की कीमत पर हुआ। दुर्भाग्यवश, हम सबने भी उसी को आगे बढ़ाया। विचारों में स्वराज की कौन कहे यहाँ ती भारत की समस्याओं की पहचान और उसके समाधान की दिशा भी विदेश से उधार ली जाने लगी। फलतः पश्चिमी दुनिया में हो रहे शोध के चालू फैशन से शोथ की समस्याओं को उधार लिया गया या फिर यहीं की समस्याओं को पश्चिमी सिद्धांतों के अनुसार ढालकर समझने की कोशिश की गई। ऐसी स्थिति में अधिकांश समाज विज्ञानों के पाठ्यक्रम भास्तीय परिस्थितियों में स्थापित ही नहीं हैं। हो, भारतीय परिस्थितियों उन सिद्धांतों के उदाहरण के रूप में रखी जाती है या फिर भारतीय उदाहरणों की व्याख्या में पाश्चात्य सिद्धांतों और अवधारणाओं के उपयोग में आने वाली कठिनाइयों को प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह ज्ञान की कलमें लगाई जाती रहीं, पर वह प्रयास बहुत फलप्रद नहीं हो सका।
यह सही है कि कई सहस्र वर्षों की विस्तृत अवधि में भारतीय इतिहास में यहाँ के समाज ने अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं, और उसमें परिवर्तन आए हैं, फिर भी यहाँ विद्यमान सांस्कृतिक निरंतरता के भी पर्याप्त प्रमाण प्राप्त होते हैं। स्थापत्य और वास्तु के भौतिक अवशेष, संगीत की स्वर लहरियों, योग के अभ्यास, आयुर्वेद की चिकित्सा, भारत के शास्नीय चिंतन, दर्शन, लोक-व्यवहार और उसकी विभिन्न परंपराओं में ऐसे अनेक सूत्र विद्यमान हैं जो समृद्ध भारतीय परंपरा की सतत उपस्थिति दर्ज कराते हैं। यहाँ तक्षशिला, विक्रमशिला, ओदंतपुरी और नालंदा जैसे विश्वस्तरीय शिक्षा केंद्र भी थे और विश्व व्यापार में अच्छी भागीदारी भी हुआ करती थी। यह सब तो अब इतिहास बन चुका है, पर इसी क्रम में विपुल ज्ञान-राज्ञि और उसके विविध प्रकार के अनुप्रयोग की विशाल परंपरा अभी भी जीवित है। इनके माध्यम से उपलब्ध एक समृद्ध विरासत के वारिस होने पर भी वह आज हमें सहज रूप में प्राप्त नहीं है। दो सदियों के अंग्रेजी शासन में स्थापित शिक्षा नीति द्वारा जो व्यवस्था स्थापित हुई और संचालित हुई उसमें शिक्षित और प्रशिक्षित अधिसंख्य भारतीय न केवल इस व्यापक परंपरा से दूर होते चले गए, बल्कि उनमें इस परंपरा के प्रति विकर्षण भी पैदा हुआ। इस परंपरा को शिक्षा की मुख्य धारा में स्थान न देकर अलग रखा गया और उसकी उपादेयता को चिना बिचारे अस्वीकृत कर दिया गया। इन सबके वलते सांस्कृतिक साक्षरता घटने लगी और जो अपना या वह पराया होता गया। धीरे-धीरे भारत के बारे में बात करना भावुकता और उसे प्रश्नों के घेरे में डालना बुद्धिवाद की निज्ञानी बनता गया। फलतः एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में भारत के बारे में हमारी रुचि कम होती गई। इस तरह की उदासीनता का परिणाम हुआ भारत की समदा को लेकर संशच और अज्ञान की वृद्धि। अब स्थिति यह हो रही है कि देश की परंपरा और संस्कृति को जानने वाले भारतविद् विशेषज्ञ बाहर से बुलाने पड़ रहे हैं।
राजनैतिक हलकों में अब राष्ट्रीयता के सवाल को लेकर कई तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं और भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ भी दी जा रही है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रीयता केवल भावना का ही प्रश्न नहीं है। उसके बौद्धिक और व्यावहारिक पक्ष भी हैं जिन पर पूर्वाग्रहमुक्त होकर बुद्धिसंगत विचार की अपेक्षा है। चूंकि राष्ट्र के साथ भावनाओं और राजनैतिक उपयोगों का दबाव बहुत ज्यादा होता है इसलिए उसे लेकर कुंठा और क्षोभ भी पैदा होते हैं। इसके अनेक उदाहरण स्वायत्तता की माँग करने वाले क्षेत्रीय आंदोलनों के रूप में हमारे सामने हैं। राष्ट्र की अखंडता की रक्षा और क्षेत्रीय स्वायत्तता के आग्रह के चीच द्वंद, तनाव, आंदोलन और हिंसा के रूप में उभरते रहे हैं। देश में अनेक प्रांतों का गठन इसी तरह के संघर्षों के सस्ते हुआ है। वस्तुतः अपने समुदाय के प्रति लगाव एक आदिम प्रवृत्ति है जो कदाचित आनुवंशिक सी लगती है अर्थात उससे मुक्ति संभव नहीं है। आज भी समूह के लगाव और उसकी उपलब्धि को सार्वभौमिक रूप से उत्सवपूर्वक उल्लास के साथ मनाया जाता है और क्षेत्रीयता की यह आदिम रुज्ञान कभी-कभी उन्माद के स्तर तक पहुंच जाती है।
राष्ट्रीयता मूल रूप से पहचान की भी चुनौती है। साथ ही यह 'अपने' और 'पराए' के भेद से भी जुड़ी है। हमारी अपनी विशिष्टताएँ दूसरों से अलग करती है। समूह की समृद्धि, आकार और उपसमूहों की संख्या भी इस भेद को निर्धारित करती है। परिवेश के साथ अनुकूलन और बाह्य संपर्क का स्वरूप भी पहचान को प्रभावित करते हैं। इसी तरह, जब किसी बड़े समाज के कुछ भाग अन्य भागों से संवाद नहीं कर पाते हैं तो भाषा, मूल, धर्म आदि के आधार पर छोटे आकार के स्वतंत्र समूहों का निर्माण होने लगता है। इस तरह से उपजे अज्ञान और संवादहीनता के कारण भावनात्मक टूट पैदा होती है और अलग-अलग राष्ट्रीयताएँ उमरने लगती हैं। वैसे, अपने समूह के प्रति लगाव विलकुल स्थिर भी नहीं रहता। बाहरी आक्रमण का भय अकसर लगाव या वफादारी का दायरा घटा-बढ़ा देता है। अपने पराए की श्रेणियों भी स्थायी नहीं होती। जव समूह उन्नति की दिशा में आगे बढ़ता है तो अधिकाधिक लोगों को अपने में शामिल करता चलता है, परंतु पराभव की स्थिति में संकुचन की प्रवृत्ति प्रबल होने लगती है। भिन्न-भिन्न समूहों की अस्मिताएं इसलिए भी टकराने लगती हैं कि एक की विशेषता दूसरे द्वारा अपने लिए खतरे के रूप में देखी जाने लगती है।
राष्ट्रीयता के बोध हेतु परंपरा, भाषा, इतिहास, प्रथाएँ, रीति-रिवाज और अनुष्ठान आदि में साझेदारी और समानता अपेक्षित होती है। वर्तमान में जो प्रचलन है उसके मुताविक राष्ट्र वस्तुतः राष्ट्र-राज्य (नेशन स्टेट) तक ही सीमित है जिसका अपने निर्धारित क्षेत्र में असीमित अधिकार और सार्वभौम सत्ता स्वीकार्य होती है। यूरोप में इस तरह के राष्ट्र राज्यों का गठन शुरू हुआ। राज्य में लोकतांत्रिक दृष्टि से जब जन इच्छा का प्रतिनिधित्व स्थापित हो जाता है तो अनिवार्य रूप से सभी नागरिकों को उसका निष्ठापूर्वक पालन करना होता है। ऐसा न करना राष्ट्रद्रोह कहलाता है। राष्ट्र-राज्यों के विकासक्रम को देखें तो वहाँ समूह के मूल (ओरिजिन) की एकता की स्वीकृति, वाहे वह मिथकीय या कल्पित ही क्यों न हो, प्रमुखता से उपस्थित पाई जाती है।
जब भारतवर्ष पर दृष्टिपात करते हैं तो पता चलता है कि राष्ट्र-राज्य की आधुनिक राष्ट्र-चेतना का सीधा संबंध अंग्रेजी राज के विरोध से है। उसी क्रम में यह चेतना पनपी। इस अर्थ में हम विश्व के अन्य उपनिवेशों जैसी ही स्थिति पाते हैं। राष्ट्र राज्य के रूप में भारत एक समर्थ देश बनने की अभिलाषा रखता है। पर यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में 'राष्ट्र' की अवधारणा हजार साल से ज्यादा पुरानी है। वैदिक साहित्य, विशेषतः ऋग्वेद के पृथ्वी सूक्त, में उल्लिखित 'अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां' आदि मंत्रों में राष्ट्र की चर्चा का बड़ा ही महत्वपूर्ण संदर्भ मिलता है। निश्चय ही यह राष्ट्र-राज्य की सीमित भावना से अलग एक व्यापक अवधारणा थी जो देश काल के एक व्यापक सांस्कृतिक बोध और विश्व दृष्टि में अवस्थित थी।
ऐतिहासिक रूप से भारत में आर्य, द्रविड़, मंगोल आदि विभिन्न मूलों के जोग आते रहे हैं और भारत के विभिन्न भागों में कुछ इस तरह मिल-जुलकर रहते रहे कि उनकी स्वतंत्र पहचान लगभग असंभव-सी हो गई। समाज में स्तर-विभाजन हुआ। वर्ण और जाति के स्तर भेद बने, पर एक बड़े भाग में समाज में सहअस्तित्व बना हुआ था। सामूहिक तौर पर इस स्तर भेद की सीढ़ी पर ऊपर-नीचे आना-जाना संभव होता था। विभिन्न समूहों के बीच परस्पर निर्भरता भी थी और एक साली सांस्कृतिक चेतना निश्चित रूप से विद्यमान थी। विभिन्न जन समूह देश के विभिन्न प्रांतों में आते-जाते रहे। समूचा भारत, उसकी धरती, पहाड़, नदियों, द्वारने और वनस्पतियों सभी के साथ एक गहरा और पवित्र भाव जुड़ा हुआ था। सब-के-सब देवी-देवताओं की उपस्थिति से अनुप्राणित भाव की अनुभूति कराते थे।
भारत की पहचान हिमालय और सागर के आधार पर की जाती रही। गंगा, गोदावरी, कावेरी, शिप्रा, मंदाकिनी, सरयू जैसी नदियों पुण्यदायी मानी गई। जगन्नाथपुरी, द्वारिका, काशी, कोंची, उज्जैन, मथुरा और अयोध्या नगरियों को मोक्षदायिनी माना गया। विचारों और आंदोलनों की दृष्टि से पूरा भारत दृष्टि में रहा। सुदूर दक्षिण के शंकराचार्य ने अपने केंद्र श्रृंगेरी, पुरी, द्वारिका और बदरीनाथ में स्थापित किए। आज भी बदरिकाश्रम की पूजा-अर्चना एक नम्बूदरी पुजारी ही करते हैं। बाद में भक्ति की धारा पूरे देश में प्रवाहित हुई और अपूर्व काव्य-रचनाएँ प्रकाश में आई। कला के क्षेत्र में समूचे भारत में कुछ प्रवृत्तियों दिखती हैं। ओडिशा में खंडगिरि-उदयगिरि और कोणार्क, महाराष्ट्र में अजंता एलोरा तथा तमिलनाडु के महाबलीपुरम और तंजावुर का वृहदीश्वर मंदिर, मदुरै और खजुराहो के मंदिर आदि मिन्न-भिन्न स्थानों पर पहुँचकर यही लगता है कि भारत की एक छाप इन सभी जगहों पर है। कोई एक तरह का कला-बोध है जो इन सभी भिन्न स्थानों पर साझा हो रहा है। शिल्प और चित्रकला की आभा और शैली में सर्वत्र एक-सी प्रेराणा प्रतीत होती है। सामवेद से आरंभ हुई शास्त्रीय संगीत की धारा विविध रूपों में पुष्पित और पल्लवित हुई। विभिन्न माषाओं के साहित्य में भी भारतीयता की छवि विद्यमान है।
यदि प्राचीन मतों की बात करें तो उनमें बड़े गंभीर भेद हैं। द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, वैष्णव, शाक्त, शैव, जैन, बौद्ध बादि मत हैं और प्रत्येक के उपमेद भी हैं जिनकी जटिल व्यवस्था है। शास्त्रीय ज्ञान की परंपराओं में मतभेद और शास्त्रार्थ की लंबी परंपरा है, पर इनको मानने वाले सभी अपने को भारतीय ही कहते हैं। दूसरी ओर, लोक जीवन की भी विविध परंपराएँ रही हैं और अभी भी जीवित हैं। कबीर, सूर, तुलसी, रैदास, रहीम, रसखान, जिनके बिना हिंदी की कल्पना नहीं की जा सकती, अलग-अलग धाराएँ प्रवाहित कर रहे थे और राष्ट्रीयता ऐसी थी कि सभी समाविष्ट थे। कह सकते हैं वह विकेंद्रित थी। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में राजतंत्र और गणतंत्र वाले सोलह जनपदों का उल्लेख मिलता है। पर वे यूरोप के मॉडल वाले राष्ट्र-राज्य के तर्ज पर चिलकुल नहीं थे। हमारी राष्ट्रीयता की अवधारणा आक्रामक और असहिष्णु नहीं थी। इसका प्रमाण है शक, हूण, कोल, किरात सबको उनकी मूल, भाषा और जीवन-शैली की भिन्नता के बावजूद अवसर देना। इन सबके साथ इतना मिश्रण हुआ है कि शुद्ध जाति का निश्चय ही संभव नहीं रहा। भारतीयता की उपस्थित्ति निश्वय ही यहाँ के जीवन मूल्यों में है जिसकी आधुनिक परिणति महात्मा गाँधी में मिलती है। सत्य और अहिंसा को जीवन-धर्म बनाना और सकल सृष्टि के साथ निकटता ही हमारी और मनुष्य मात्र की पहचान होनी चाहिए क्योंकि पृथ्वी माता है और हम सब उसकी संतान हैं। देश के साथ मातृवत संबंध होना चाहिए।
भारत और भारतीयता पर चर्चा समकालीन सांस्कृतिक विमर्श में एक चुनौती भरा काम हो गया है। यह चुनौती तव और भी बढ़ जाती है जब कोई भारतीय भारत के बारे में बात करे, वह भी जिसे घोषित भारतवादी करार दिया गया हो। पर भारत को भारत के नजरिए से अर्थात यहाँ की व्यापक सांस्कृतिक दृष्टि से देखने की शुरुजात तो करनी ही पड़ेगी। इस कार्य के लिए आचार्य विद्यानिवास मिश्र का चिंतन एक सार्थक प्रस्थानविंदु के रूप में उपस्थित होता है। वे संस्कृत और भाषा विज्ञान के पंडित, श्रेष्ठ हिंदी निबंधकार होने के साथ भारतीय संस्कृति के गंभीर अध्येता भी थे। भारत और विदेश में अध्ययन, अध्यापन, भ्रमण और सांस्कृतिक संपर्क के आलोक में मिश्र जी ने भारत विषयक चिंतन को प्रखर रूप से उपस्थापित किया है। आशा है इस संकलन के निबंध पाठकों को भारत के स्वरूप को निकट से समत्राने में सहायक होंगे और इस दिशा में उनकी रुचि बढ़ाएंगे।
- गिरीश्वर मित्र