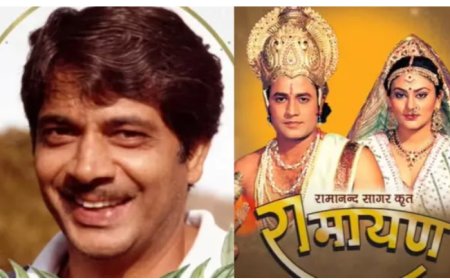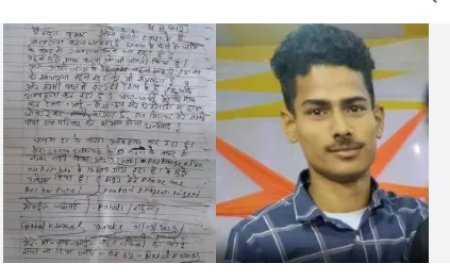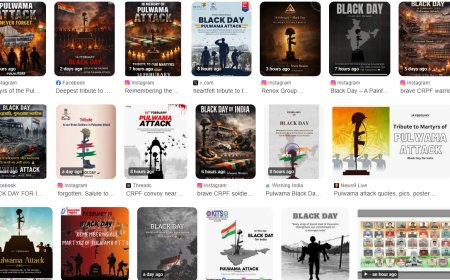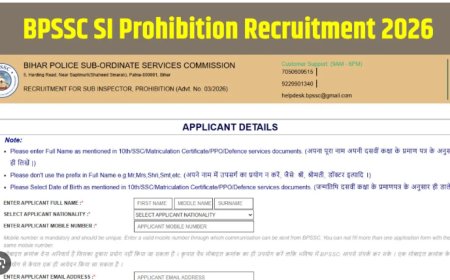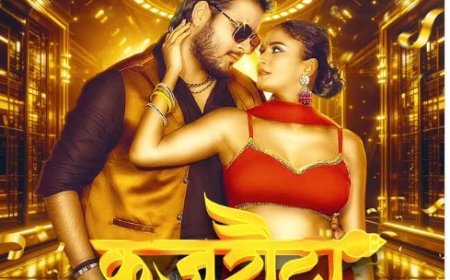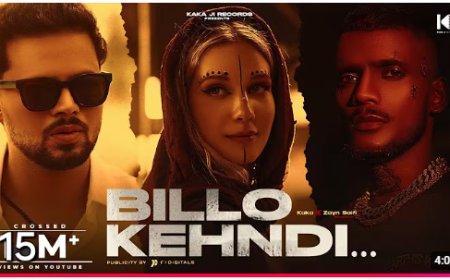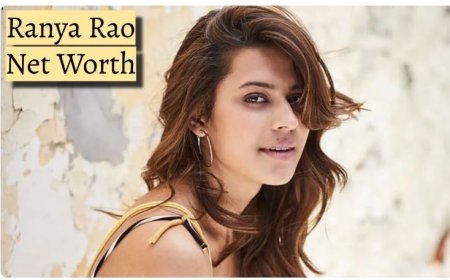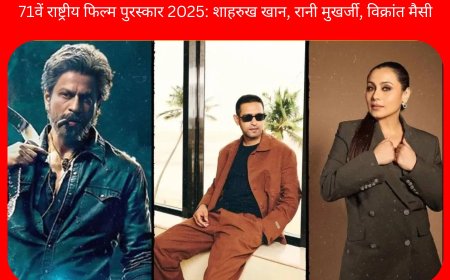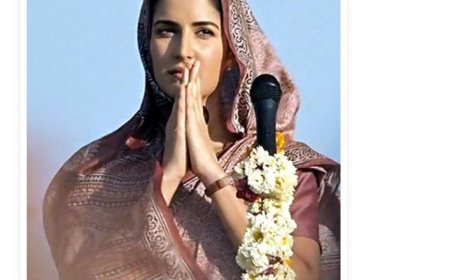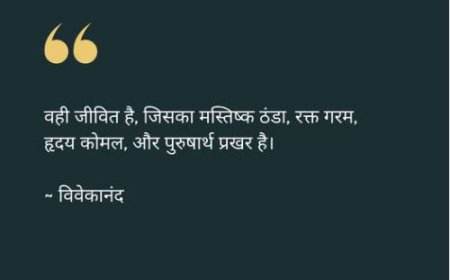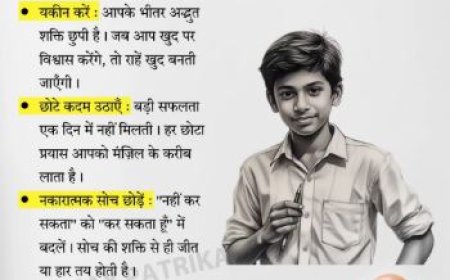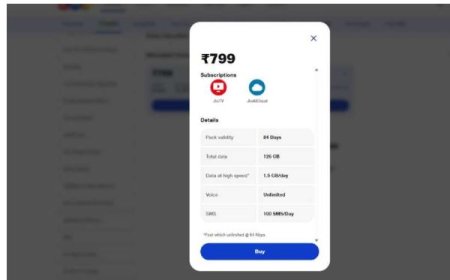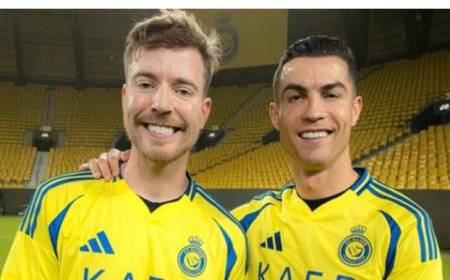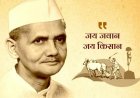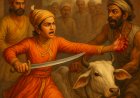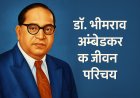पराली जलाने की बढ़ती समस्या और समाधान के रास्ते
उत्तर भारत में पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जानिए कैसे मशीनों के बेहतर प्रबंधन, जागरूकता, एक्स-सीटू उपयोग और किस्म परिवर्तन से इस समस्या का स्थायी समाधान संभव है।

यह विषय उत्तर भारत में पराली जलाने की समस्या और उसके स्थायी समाधान पर केंद्रित है।
पराली जलाने से उपजता धुआं: समाधान के रास्ते
हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीनों में उत्तर भारत के आसमान में धुंध और धुएं की मोटी परत छा जाती है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के खेतों में किसानों द्वारा जलाई गई पराली इस प्रदूषण का बड़ा कारण बनती है। बीते सात वर्षों में सरकारों ने फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के वितरण से लेकर जैव ईंधन परियोजनाओं और जुर्माने जैसे कई उपाय किए, लेकिन आर्थिक सीमाओं, व्यवस्थागत खामियों और जागरूकता की कमी के कारण यह समस्या अब भी ज्यों की त्यों बनी हुई है।
दिल्ली की हवा की निगरानी करने वाले एयर क्वालिटी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अनुसार, पराली जलाने के चरम समय यानी अक्टूबर-नवंबर में दिल्ली के पीएम 2.5 प्रदूषण में 15 से 30 प्रतिशत तक इजाफा होता है। इसलिए, इस समस्या का स्थायी समाधान पंजाब और हरियाणा में समन्वित प्रयासों के बिना संभव नहीं है। यदि अगले तीन वर्षों तक लगातार और साझा प्रयास किए जाएँ, तो वर्ष 2028 तक प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय कमी लाना संभव होगा।
सुधार के लिए ज़रूरी कदम
पहला कदम फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की उपलब्धता और उपयोग को सुचारु बनाना है। पंजाब और हरियाणा में लगभग ढाई लाख मशीनें हैं, जो सैद्धांतिक रूप से सभी गैर-बासमती धान के खेतों को कवर कर सकती हैं, परंतु कस्टम हायरिंग सेंटरों (CHC) की किराये की व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी के कारण यह व्यवस्था केवल 40 प्रतिशत क्षमता पर काम कर रही है। सरकारों को तकनीकी प्रशिक्षण, मशीनों के रखरखाव और ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि हर किसान तक सुविधाएं सहजता से पहुँचें।
दूसरा कदम किसानों में जागरूकता बढ़ाना है। कई किसान यह मानते हैं कि मशीनों से अवशेष प्रबंधन करने पर कीटों की समस्या बढ़ती है या उपज घटती है, जबकि ऐसा नहीं है। इस मिथक को तोड़ने के लिए राज्यों को अपने फसल अवशेष प्रबंधन बजट का कम से कम पांच प्रतिशत सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों पर खर्च करना चाहिए। खेतों में प्रदर्शन, किसानों के सफल उदाहरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम इस दिशा में सहायक हो सकते हैं।
तीसरा बड़ा उपाय एक्स-सीटू (Ex-situ) तरीकों का विस्तार है। इसमें पराली का उपयोग बायोगैस, बायोचार या औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है। पंजाब ने 2023 में लगभग 60 प्रतिशत क्षमता तक ऐसे प्रबंधन का लक्ष्य हासिल किया था, परंतु आपूर्ति श्रृंखला, भंडारण और तकनीकी कर्मियों की कमी अब भी बड़ी बाधा है। राज्यों को बायोमास की उचित कीमत तय करनी होगी ताकि किसानों को भी आर्थिक लाभ मिले और उद्योगों को स्थायी ईंधन संसाधन मिल सके।
नए अवसर और वैकल्पिक दृष्टिकोण
बायोचार और किण्वित जैविक खाद जैसे उत्पाद किसानों के लिए नए आय स्रोत बन सकते हैं। इनके मानकीकरण, बाजार विकास और कार्बन क्रेडिट प्रणाली के माध्यम से भारत इन उत्पादों को वैश्विक स्तर पर भी बेच सकता है। साथ ही, कृषि विश्वविद्यालयों को इन उत्पादों के उपयोग के दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए ताकि किसान इन्हें समझकर अपनाएं।
अंततः, धान की परंपरागत किस्मों में परिवर्तन भी आवश्यक है। पूसा 44 जैसी किस्में अधिक पराली और जल की खपत करती हैं, जबकि पीआर 126 जैसी अल्प अवधि वाली किस्में बेहतर विकल्प हैं। सरकार यदि अनाज खरीद सीमा को स्थानीय औसत उपज के अनुसार तय करे, तो किसानों को स्वाभाविक रूप से कम पराली देने वाली किस्में उगाने के लिए प्रेरणा मिलेगी।
पराली जलाना केवल किसानों की समस्या नहीं है, यह पर्यावरण, स्वास्थ्य और नीति-निर्माण से जुड़ा सामूहिक विषय है। जुर्माने लगाने से ज्यादा ज़रूरी है कि किसानों को तकनीकी, आर्थिक और शैक्षिक सहायता दी जाए। सरकार, उद्योग, शिक्षा संस्थान और किसान – सभी मिलकर एक स्थायी प्रणाली विकसित करें। तभी दिल्ली और उत्तर भारत की हवा फिर से साफ और सांस लेने योग्य बन सकेगी।